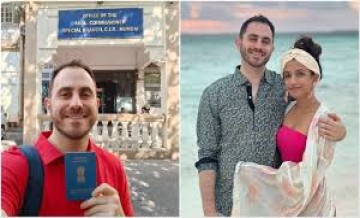#100Women: ट्रांसजेंडर होने के दंश से लड़ती वैजयंती
By Shobhna Jain | Posted on 28th Nov 2016 |
गजब दुनिया

वैजयंती वसंता मोगली, ट्रांसजेंडर वूमेन, बीबीसी हिंदी डॉटकॉम के लिए
मैं स्कूल में थी जब यौन और शारीरिक हिंसा की शिकार हुई. वयस्क होने के बाद भी मुझे बार-बार निशाना बनाया गया.
लेकिन मैंने पीड़ित महसूस करने की जगह उससे उबरने और लड़ने का रास्ता चुना.
अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए जातिगत भेदभाव वाले उस पितृसत्तात्मक समाज को ख़ारिज़ किया जो मेरे दूसरे बहादुर ट्रांसजेंडर दोस्तों की आवाज़ को बेरहमी से दबा देते हैं. ये मेरी कहानी है.
12 साल की उम्र तक, मैंने उन लोगों से मिलना-जुलना और बतियाना शुरू कर दिया था, जिन्हें समाज में हिजड़ा कहा जाता है. इस तरह ही मेरे रिश्तेदारों को मेरे ट्रांसजेंडर होने का पता चला.
हैदराबाद में मेरे स्कूल का अनुभव बहुत ख़राब रहा. वहां मेरे कुछ सीनियर मुझे अपने जैसा नहीं पा कर हमेशा मेरा शारीरिक और यौन उत्पीड़न करते थे.
16 साल की उम्र में, मेरे पिता ने सज़ा के तौर पर सर्दी की एक रात में अपने घर से निकाल दिया, ताकि मेरी 'अकल ठिकाने' आ जाए. उन्होंने कहा था, "सर पे छत नहीं होगी तो तेरी बदमाशियां ठिकाने आ जाएगी."
जीवन में पहली बार मैं बेघर थी. मैंने सिर्फ़ दसवीं क्लास तक पूरी पढ़ाई की है, उसके बाद 'डिसटैन्स एजुकेशन' के ज़रिए पढ़ाई पूरी की. मुझे काफ़ी जल्दी काम करना शुरू करना पड़ा था.
अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए सेक्स वर्क तक किया. ये वो दौर था, जब मेरी ज़िंदगी बेघर होने, सड़कों पर रात बिताने, दोस्तों, कुछ भले रिश्तेदारों और मेरे माता-पिता के यहां रहने के बीच कट रही थी.
एक दिन जब मैं अपने माता-पिता के घर थी, सुबह उठने पर मैंने ख़ुद को बंधा हुआ पाया. मेरे पिता ने कुछ दूसरे लोगों की मदद से मुझे जबरन एक मनोचिकित्सा वाले सेंटर में दाखिल करा दिया.
20 साल की उम्र में, मेरा जबरन मेडिकल इलाज किया गया, जो एक तरह से लिंग बदलने या समलैंगिकता से उबारने की थेरेपी के नाम पर 'फ्रॉड' ही था. मुझे आठ महीने तक ज़बर्दस्ती पागलपन रोकने वाली दवा दी गई, बिजली के झटके दिए गए. इन सबका मेरे स्वास्थ्य और मनोबल पर बुरा असर पड़ा.
इसके बाद मैं घर से मुंबई भाग गई. काफ़ी मुश्किल से किसी तरह इकॉनामिक्स में बी.ए. करने में कामयाब हुई. इसके बाद मैंने बीपीओ में काम करना शुरू किया. 32 साल की उम्र होने तक मैं घर नहीं लौटी, लेकिन नियमित तौर पर माता-पिता को पैसे भेजती रही.
मैं 2012 में तब घर लौटी जब मेरी मां को पार्किंसन और अल्जाइमर्स की बीमारी हुई. 2013 में मेरे पिता ने कोई 'जादुई दवा' मेरे खाने में मिला दी, उस दवा पर उन्हें भरोसा था कि इसके खाते ही मैं पुरुष बन जाऊंगी.
मैं तब बेहद घातक ड्रग रिएक्शन, 'टॉक्सिक एपिडरमन नेक्रोलिस' (टीईएन) का शिकार हो गई थी. जले हुए मरीजों का जिस तरह इलाज होता है, वैसे ही महीनों तक मेरा इलाज चला.
जनवरी 2014 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को गैर आपराधिक ठहराने के मामले में कौशल की पुर्नविचार याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में अवैज्ञानिक, अनैतिक और प्राय धोखाधड़ी भरे मेडिकल इलाज और प्रैक्टिस के ख़िलाफ़ मैंने गवाही दी.
जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों को अलग जेंडर के तौर पर पहचान दी, तब मैंने अपने ऑफ़िस में आधिकारिक तौर पर अपना जेंडर बदलवाने की कोशिश की और उसके बाद से ही मैं बेरोज़गार हूं.
ट्रांसजेंडर समुदाय में बेरोज़गारी दुनिया भर में देखने को मिलती है. कुछ ट्रांसजेंडरों नौकरी में ज़रूर पहुंचते हैं लेकिन उन्हें नौकरी ट्रांसजेंडर के तौर पर नहीं मिली होती है बल्कि उस नाम और जेंडर के आधार पर मिली होती है जो उनके जन्म के दौरान दिया जाता है.
ट्रांसजेंडर, प्रमाणपत्र में अपना जेंडर बदलवाने की की कोशिश करते हैं तो ज़्यादातर लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ता है.
मैं पहले जिस कंपनी में काम करती थी वो, 'वॉल स्ट्रीट' की बहुत बड़ी कंपनी है और उसका ग्लोबल दावा है कि वह 'एलजीबीटीआईक्यू' समुदाय के प्रति समावेशी नज़रिया रखती है. लेकिन इस कंपनी में मुझे महिला शौचालय के इस्तेमाल की इज़ाजत नहीं दी गई.
मुझे पुरूषों के शौचालय के इस्तेमाल के लिए मज़बूर किया गया, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई सरकारी पहचान पत्र नहीं था जो मेरे ट्रांसजेंडर होने की तस्दीक करता.
दुनिया भर के कई देशों में, ख़ासकर विकसित देशों में ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित वर्ग में रखा जाता है और उनके प्रति भेदभाव रहित मापदंड अपनाने होते संवैधानिक निर्देश होते हैं. लेकिन भारत में ट्रांसजेंडरों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है.
हिम्मत की मिसाल
मैं अपना जेंडर बदलवाने के लिए राज्य सरकार को काफी पहले आवेदन दे चुकी हूं लेकिन कई महीने बीतने और कई बार 'फॉलोअप' करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला है.
समाज के हाशिए पर धकेल दिए जाने की सूरत में हमारे पास केवल अदालत का विकल्प बचता है लेकिन मुक़दमेबाज़ी के लिए जरूरी संसाधन हम में से कईयों के पास नहीं होते.
बेरोज़गारी की स्थिति में मैंने, प्रतिष्ठित 'टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ़ सोशल साइंस', हैदराबाद में लोकनीति के पाठ्यक्रम में नामांकन कराया, लेकिन मेरे माता-पिता गंभीर रूप से बीमार हैं. उन्हें हमेशा देखभाल करने वाले की जरूरत है.
ज़्यादातर ट्रांसजेंडरों के लिए पूर्णकालिक पढ़ाई, लग्ज़री से कम नहीं होती. माता पिता के इलाज के बढ़ते मेडिकल बिल और इसके चलते बढ़ते कर्जे के कारण मैं पढ़ाई जारी नहीं रख पाने को विवश हूं.
मैं ऐसी अर्थव्यवस्था में बेताबी से नौकरी ढूंढ़ रही हूं जो ट्रांसजेंडरों को नौकरी नहीं देती. हालांकि काफ़ी देरी से ही सही लेकिन मेरे पिता अब कहते हैं, "मुझे अचरज होता है कि अपने रिश्तेदारों पर भरोसा करके मैं ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था, वे अब कहीं नहीं हैं और तुम मेरी देखभाल के लिए यहां मौजूद हो."
मैं शुक्रगुज़ार हूं कि देर से ही सही जीवन ने अब तो मुझे अपने मां-बाप के पास रहने का मौका दिया है.
source: BBC Hindi.Com
Leave a Comment:
No comments found. Be a first comment here!